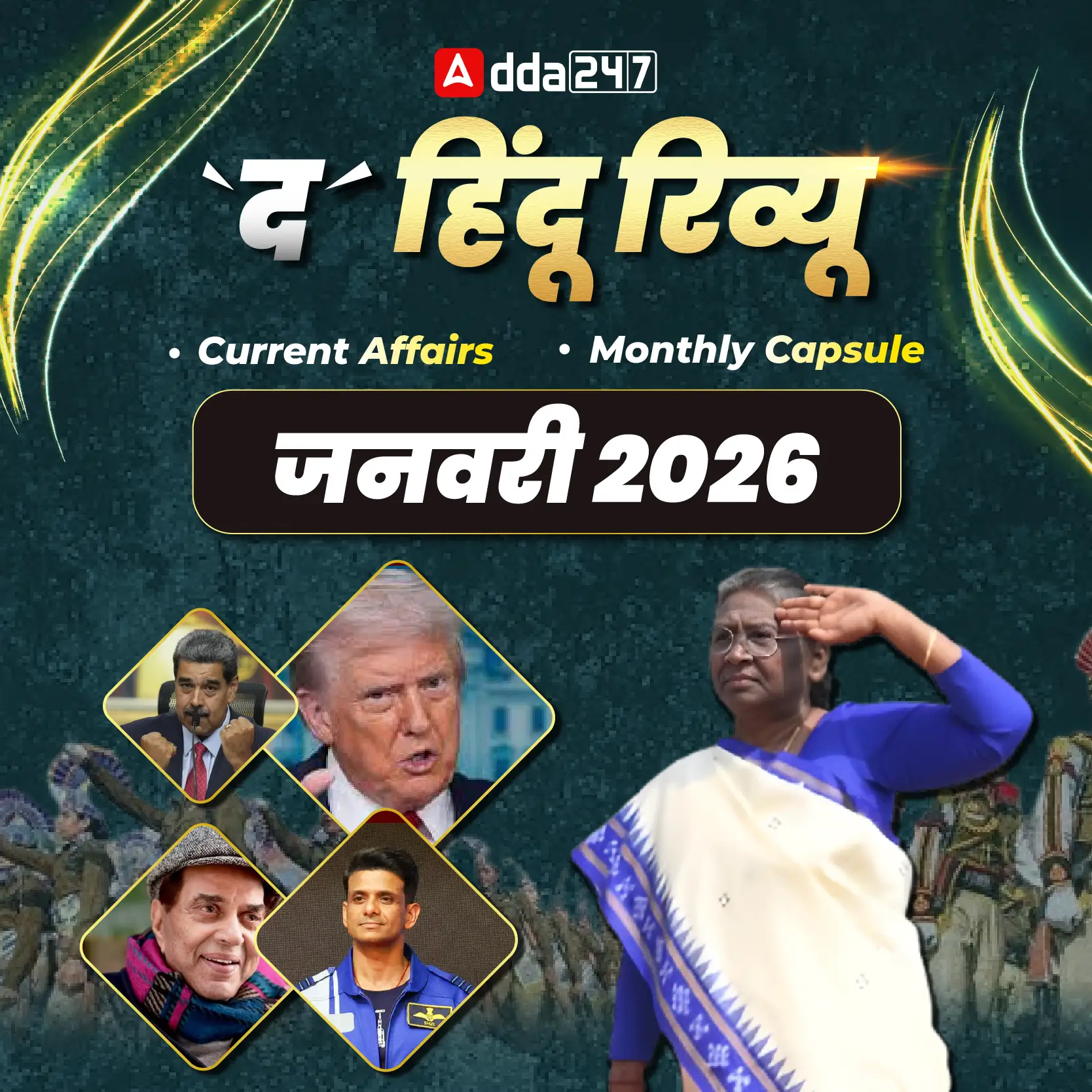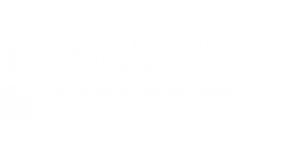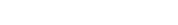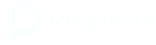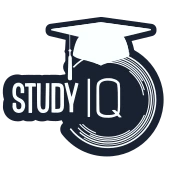संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइज़ेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता ने आधिकारिक रूप से टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया है। अनुमानित 4.2 करोड़ आबादी के साथ, इंडोनेशिया की राजधानी अब तेजी से बढ़ते एशियाई मेगासिटीज़ की सूची में शीर्ष पर आ गई है।
यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र के नए और मानकीकृत शहरी परिभाषा मानदंडों के कारण आया है, जिनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शहरी आबादी के आकलन के लिए अधिक समान और तुलनीय पद्धति प्रदान करना है। यह रिपोर्ट शहरीकरण, प्रवास और जनसांख्यिकीय वृद्धि में हो रहे बदलावों को दर्शाती है, और नीति-निर्माताओं तथा शहरी विकास के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है।
शीर्ष रैंकिंग: वर्ष 2025 में दुनिया के 3 सबसे अधिक आबादी वाले शहर
-
जकार्ता (इंडोनेशिया) – 4.2 करोड़
-
ढाका (बांग्लादेश) – 3.7 करोड़
-
टोक्यो (जापान) – 3.3 करोड़
2018 की पिछली UN रिपोर्ट सहित कई दशकों तक शीर्ष स्थान पर रहने वाला टोक्यो अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है, हालांकि यह अभी भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण महानगरीय क्षेत्रों में से एक है।
UN की नई कार्यविधि में क्या बदला?
इस रैंकिंग में बदलाव का मुख्य कारण संयुक्त राष्ट्र के अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा शहरी सीमांकन मानकों में सुधार है। पहले के आकलन विभिन्न देशों की प्रशासनिक परिभाषाओं पर निर्भर थे, जिससे टोक्यो जैसे बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों वाले शहरों को लाभ मिलता था।
नई पद्धति में शामिल हैं:
-
समान जनसंख्या घनत्व और भू-स्थानिक (geospatial) मानक
-
वास्तविक कार्यात्मक शहरी क्षेत्रों का सटीक मानचित्रण
-
शहरी विस्तार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का बेहतर आकलन
इससे जकार्ता और ढाका जैसे शहरों का वास्तविक शहरी आकार अधिक सटीक रूप से सामने आ पाया है।
तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण: एक बड़ा वैश्विक परिदृश्य
रिपोर्ट के अनुसार:
-
1950 में दुनिया की केवल 20% आबादी शहरों में रहती थी।
-
2025 में, विश्व की 8.2 अरब आबादी का लगभग आधा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रह रहा है।
-
2050 तक, दुनिया की जनसंख्या वृद्धि का दो-तिहाई हिस्सा शहरों में होगा।
मेगासिटीज़ (जनसंख्या ≥ 1 करोड़) की संख्या 1975 में 8 से बढ़कर 2025 में 33 हो गई — यानी पाँच दशकों में चार गुना वृद्धि।
एशिया का दबदबा
अब दुनिया के 10 में से 9 सबसे अधिक आबादी वाले शहर एशिया में हैं:
-
जकार्ता
-
ढाका
-
टोक्यो
-
नई दिल्ली
-
शंघाई
-
ग्वांगझोऊ
-
मनीला
-
कोलकाता
-
सियोल
शीर्ष 10 में एकमात्र गैर-एशियाई शहर काहिरा (मिस्र) है।
टोक्यो की जनसांख्यिकीय बदलती कहानी
वैश्विक रैंकिंग में नीचे आने के बावजूद, टोक्यो दुनिया के सबसे प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। इसके 3.3 करोड़ लोग ग्रेटर टोक्यो एरिया (सैतामा, चिबा, कनागावा) में फैले हुए हैं — जिसमें योकोहामा (जनसंख्या: 37 लाख) भी शामिल है।
हालाँकि, यह क्षेत्र जापान की व्यापक जनसंख्या गिरावट को दर्शाते हुए धीरे-धीरे घट रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि “टोक्यो प्रॉपर”—23 विशेष वार्ड और आस-पास के शहर—की आबादी पिछले दशक में बढ़ी है, जो मुख्यतः युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए प्रवास से प्रेरित है।
जकार्ता के शीर्ष पर आने के निहितार्थ
जकार्ता की बढ़ती आबादी शहरी विकास की कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों को उजागर करती है:
-
इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव: आवास, परिवहन, स्वच्छता और जल आपूर्ति पर भारी भार।
-
पर्यावरणीय चुनौतियाँ: प्रदूषण, बाढ़ और भूमि धंसने जैसी पुरानी समस्याएँ।
-
सुशासन और समानता: शहरी विस्तार के साथ सामाजिक असमानताओं को रोकना कठिन।
-
अवसर: निवेश, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में तेज़ी — जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं।
मुख्य तथ्य (Static Takeaways)
-
रिपोर्ट: वर्ल्ड अर्बनाइज़ेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 (UN DESA)
-
जकार्ता जनसंख्या (2025): 4.2 करोड़ (रैंक 1)
-
टोक्यो जनसंख्या: 3.3 करोड़ (रैंक 3)
-
शीर्ष 3 शहर: जकार्ता, ढाका, टोक्यो
-
मेगासिटीज़ (2025): 33
-
वैश्विक शहरी आबादी (2025): ~50%
-
2050 अनुमान: दुनिया की 66% आबादी शहरों में रहेगी
-
UN अधिकारी: पैट्रिक गर्लैंड, हेड ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट्स
-
UN अंडरसेक्रेटरी जनरल: शहरीकरण को जलवायु कार्रवाई, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता के प्रमुख चालक के रूप में वर्णित किया