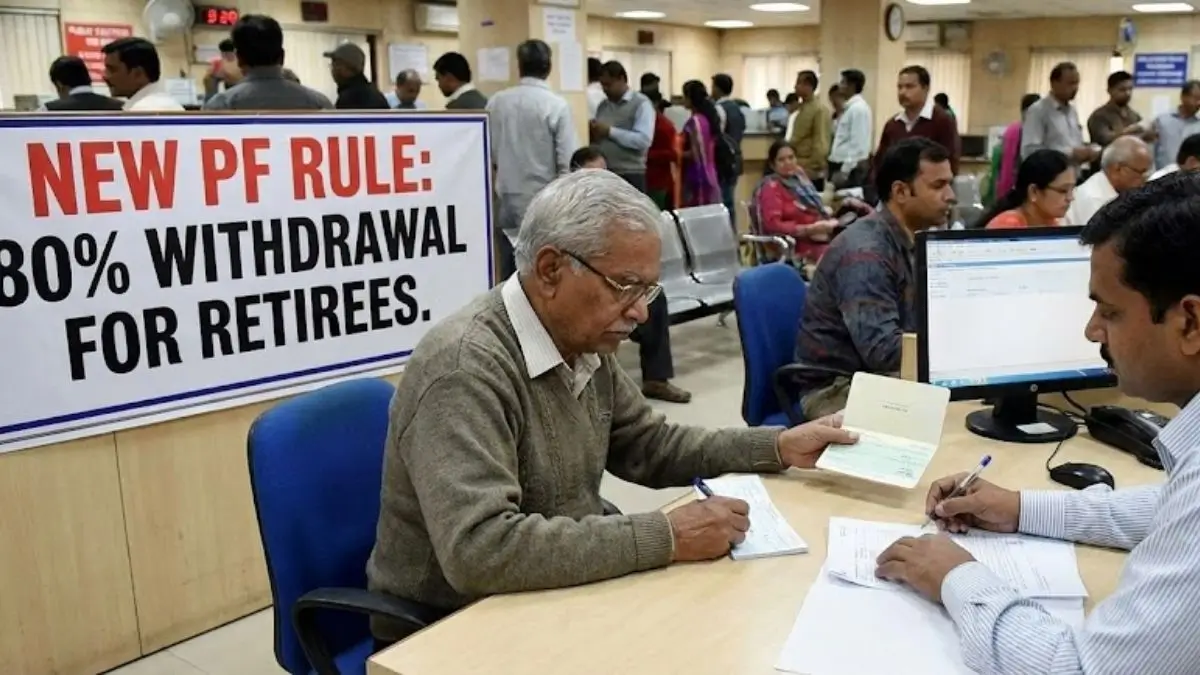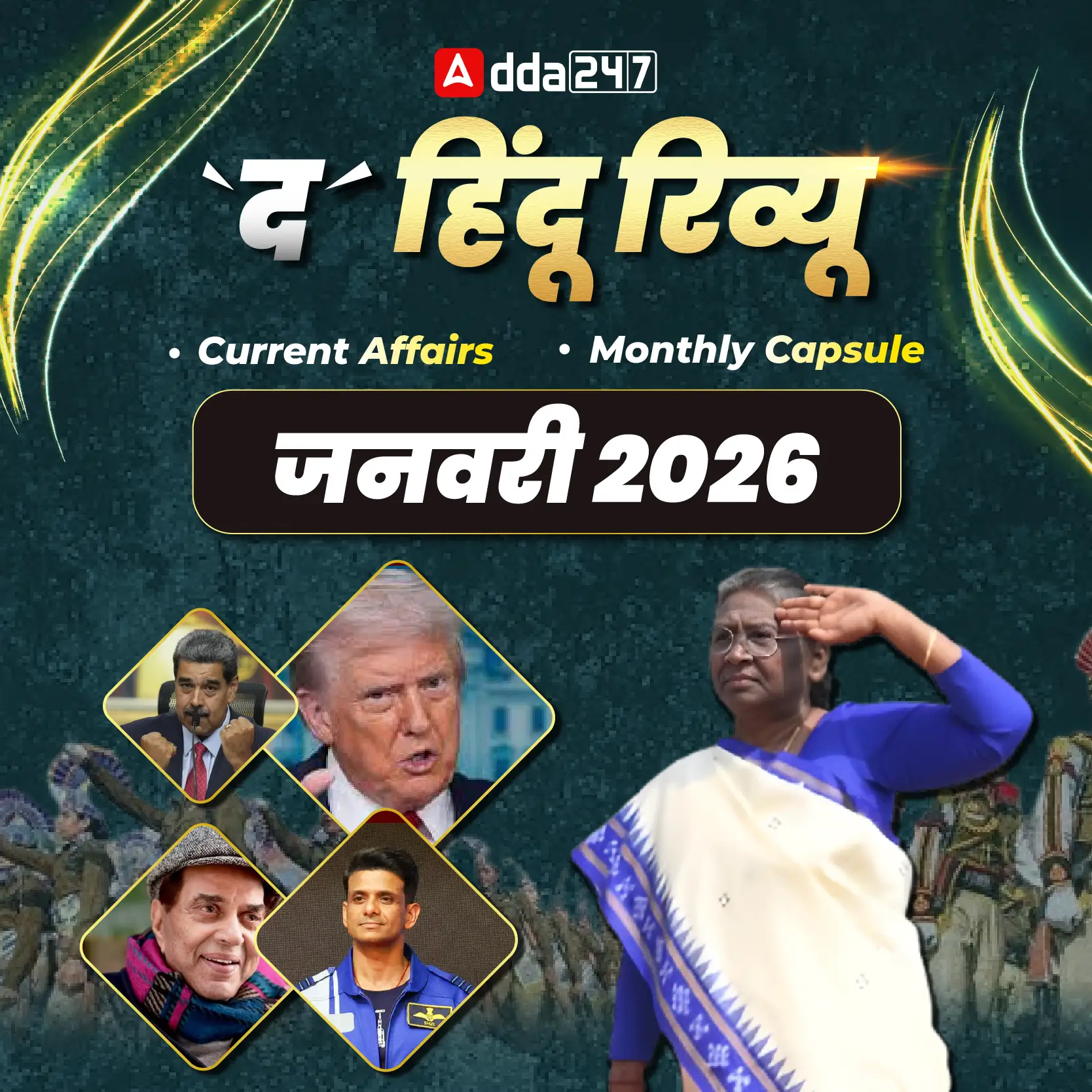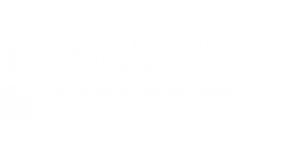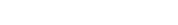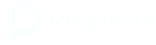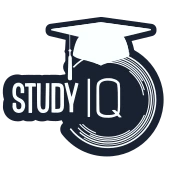फीफा बेस्ट फ़ुटबॉल अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन दोहा, क़तर में किया गया, जहाँ पिछले वर्ष विश्व फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों, गोलकीपरों, प्रशंसकों और खेल भावना के उदाहरणों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में ओस्मान डेम्बेले और आइतना बोनमती क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने।
फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025
- ओस्मान डेम्बेले (फ्रांस / पेरिस सेंट-जर्मेन) को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया।
- उन्होंने एक शानदार सीज़न के बाद यह सम्मान जीता, जिसमें वे बैलन डी’ओर भी अपने नाम कर चुके हैं।
- डेम्बेले ने पीएसजी की ऐतिहासिक ट्रेबल जीत में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसमें क्लब का बहुप्रतीक्षित यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब भी शामिल है।
- उनकी गति, रचनात्मकता और मैच जिताऊ प्रदर्शन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं।
उन्होंने निम्न खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा:
- लामिन यामल (बार्सिलोना, स्पेन)
- किलियन एम्बाप्पे (रियल मैड्रिड, फ्रांस)
- विजेता का चयन राष्ट्रीय टीम कप्तानों, कोचों, पत्रकारों और प्रशंसकों की वैश्विक वोटिंग से किया गया।
फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025
- आइतना बोनमती (स्पेन / बार्सिलोना) ने लगातार तीसरी बार फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का खिताब जीता।
- क्लब और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनका निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन निर्णायक रहा।
उन्होंने निम्न दावेदारों को पीछे छोड़ा:
- मारियोना काल्डेंटे (स्पेन)
- एलेक्सिया पुटेल्यास (स्पेन)
- यह उपलब्धि महिला फुटबॉल में बार्सिलोना और स्पेन के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है।
फीफा बेस्ट 2025 अवॉर्ड्स: पूरी विजेता सूची
पुरुष वर्ग
- फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर: ओस्मान डेम्बेले (फ्रांस / पीएसजी)
- सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर: जियानलुइजी डोनारुम्मा (पीएसजी)
- पुरुष कोच ऑफ द ईयर: लुइस एनरिक (पीएसजी)
- पुस्कास अवॉर्ड (सर्वश्रेष्ठ गोल): सैंटियागो मोंटिएल (अर्जेंटीना)
बेस्ट मेन्स XI
- गोलकीपर: जियानलुइजी डोनारुम्मा
- डिफेंडर्स: अशराफ हकीमी, विलियम पाचो, वर्जिल वान डाइक, नूनो मेंडेस
- मिडफील्डर्स: जूड बेलिंघम, कोल पामर, वितिन्हा, पेड्री
- फॉरवर्ड्स: ओस्मान डेम्बेले, लामिन यामल
महिला वर्ग
- फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर: आइतना बोनमती (स्पेन / बार्सिलोना)
- सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर: हन्ना हैम्पटन (इंग्लैंड / चेल्सी)
- महिला कोच ऑफ द ईयर: सरीना विगमैन
- मार्टा अवॉर्ड (महिला फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल): लिज़बेथ ओवाले (मेक्सिको / लीगा एमएक्स फेमिनिल)
विशेष पुरस्कार
- फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड: डॉ. एंड्रियास हारलास-न्यूकिंग (जर्मनी)
- फीफा फैन अवॉर्ड: ज़ाखो एससी के समर्थक