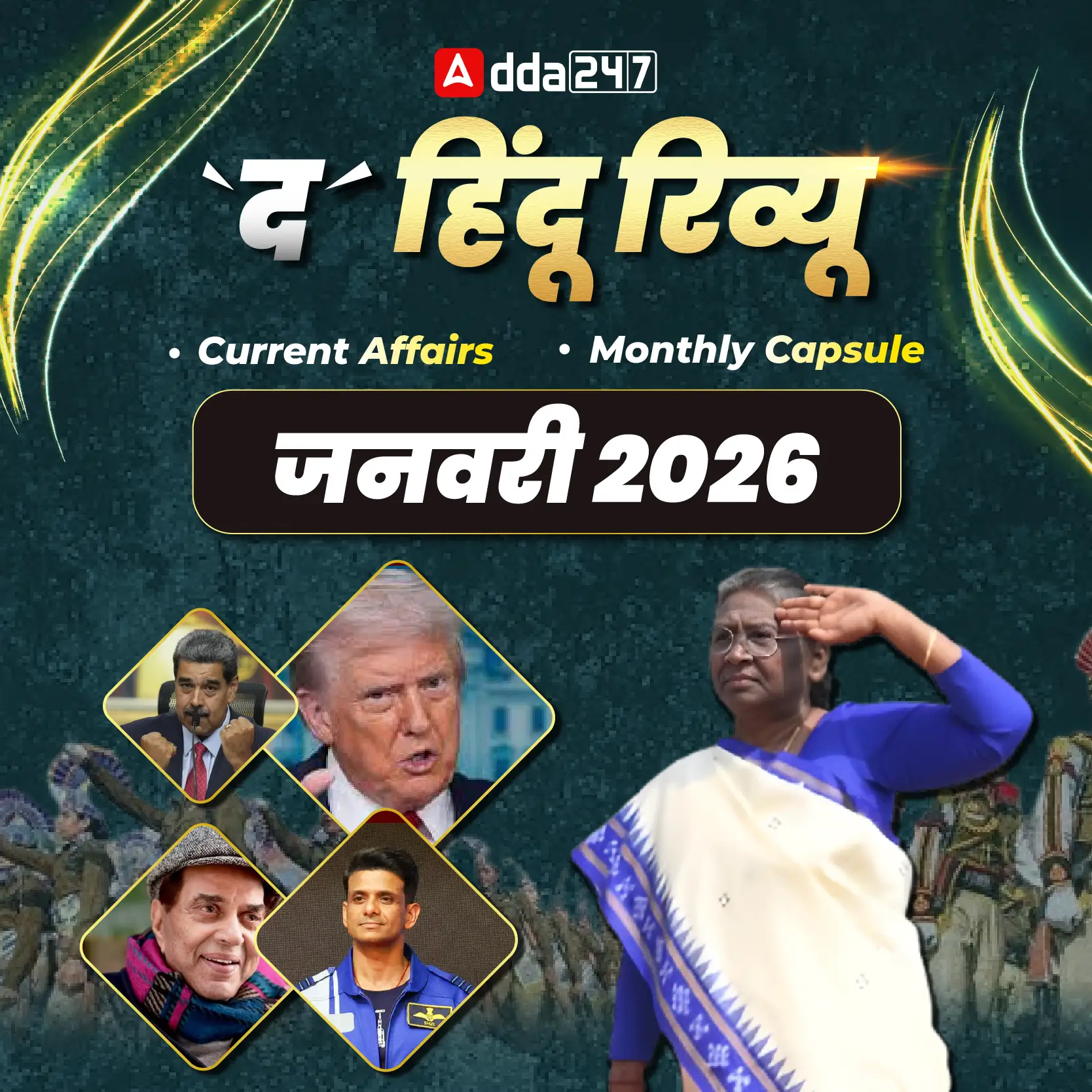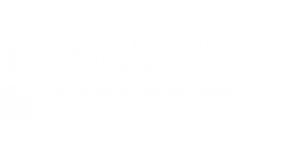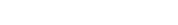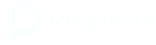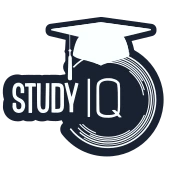केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 01 फ़रवरी 2025 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी, जिसमें भारत की वित्तीय रणनीति और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया जाएगा। वर्तमान में, केंद्रीय बजट एक व्यापक दस्तावेज़ है जो देश के व्यय और राजस्व संग्रह का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। हालांकि, यह हमेशा ऐसा नहीं था। 2017 से पहले, रेलवे बजट केंद्रीय बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था, जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही एक परंपरा थी। 2017 में, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया, जिससे भारत की बजटीय प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ।
पहले रेलवे बजट को अलग क्यों किया गया था?
1924 में, एक्वर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों के आधार पर रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और इसे एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संपत्ति के रूप में विकसित करना था। 92 वर्षों तक, रेलवे बजट केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था और इसे एक अलग वित्तीय इकाई के रूप में चलाया जाता था।
रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में क्यों मिलाया गया?
2016 में, नीति आयोग की एक समिति जिसका नेतृत्व अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय कर रहे थे, ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अलावा, बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई द्वारा लिखित एक पेपर “Dispensing with the Railway Budget” में यह सुझाव दिया गया कि रेलवे बजट को अलग रखने की परंपरा अब अपनी उपयोगिता खो चुकी है और इससे अनावश्यक जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। इन सिफारिशों के आधार पर, 2017 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया और अरुण जेटली ने पहला संयुक्त बजट प्रस्तुत किया।
विलय के प्रमुख कारण
- समग्र वित्तीय दृष्टिकोण: विलय ने सरकार की वित्तीय स्थिति को एकीकृत रूप से प्रस्तुत करने में मदद की, जिससे संसाधनों के कुशल आवंटन में आसानी हुई।
- लाभांश भुगतान की समाप्ति: रेलवे को सरकार को लाभांश (Dividend) देने से मुक्त कर दिया गया, जिससे अधोसंरचना विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध हुआ।
- “कैपिटल-एट-चार्ज” ऋण समाप्त: रेलवे पर वर्षों से लंबित सरकारी ऋण (Capital-at-Charge) को समाप्त कर दिया गया, जिससे वित्तीय दबाव कम हुआ।
- एकीकृत परिवहन योजना: इस विलय ने रेलवे, राजमार्गों और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान की।
- लचीलापन बढ़ा: वित्त मंत्रालय को बजट सत्र के मध्य समीक्षा के दौरान संसाधनों के पुनर्विन्यास की अधिक स्वतंत्रता मिली।
- सरलीकृत प्रक्रिया: एकल अनुपूरक विधेयक (Appropriation Bill) प्रस्तुत किया जाने लगा, जिससे विधायी प्रक्रिया सुगम हो गई।
विलय की प्रमुख विशेषताएँ
- रेल मंत्रालय अभी भी एक वाणिज्यिक रूप से संचालित सरकारी विभाग के रूप में कार्य करता है।
- रेलवे के लिए एक अलग बजटीय अनुमान (Statement of Budget Estimates) और अनुदान मांग (Demand for Grants) तैयार किया जाता है।
- रेलवे से संबंधित अनुमानों को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एकल अनुपूरक विधेयक (Appropriation Bill) में शामिल किया जाता है।
- रेलवे “अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों (Extra-Budgetary Resources – EBR)” के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए धन जुटा सकता है।
- यह विलय बहु-माध्यमीय परिवहन योजना (Multimodal Transport Planning) और संसाधनों के बेहतर आवंटन को बढ़ावा देता है।
विलय का प्रभाव
- दो अलग-अलग बजट प्रस्तुत करने में लगने वाले दोहराव को समाप्त किया गया।
- सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्रण हुआ।
- रेलवे को ऑपरेशनल दक्षता (Operational Efficiency) और अधोसंरचना विकास (Infrastructure Development) पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला, क्योंकि अब उसे लाभांश देने का दबाव नहीं था।
- विभिन्न परिवहन प्रणालियों (रेल, सड़क, जलमार्ग) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ, जिससे एकीकृत विकास को बढ़ावा मिला।
निष्कर्ष
रेलवे बजट का केंद्रीय बजट में विलय भारत की वित्तीय नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार था, जिसने रेलवे को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की और एकीकृत परिवहन योजना को बढ़ावा दिया। इससे रेलवे को बुनियादी ढांचे में निवेश करने, वित्तीय बोझ कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की स्वतंत्रता मिली। यह निर्णय भारत की दीर्घकालिक आर्थिक विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।



 व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर 202...
व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर 202...
 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ धीमी हुई, जनवरी मे...
कोर सेक्टर्स की ग्रोथ धीमी हुई, जनवरी मे...
 भारत में जेंडर बजटिंग में 11.55% की बढ़ो...
भारत में जेंडर बजटिंग में 11.55% की बढ़ो...